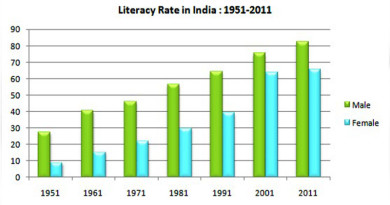साम्प्रदायिक निर्णय और पूना समझौता Communal Award and Poona Pact
24 September 1932
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेम्जे मेकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को ‘साम्प्रदायिक निर्णय’ की घोषणा की। साम्प्रदायिक निर्णय, उपनिवेशवादी शासन की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति का एक और प्रमाण था।
साम्प्रदायिक निर्णय के प्रावधान
- मुसलमानों, सिखों एवं यूरोपियों को पृथक साम्प्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया।
- आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाईयों तथा स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया।
- प्रांतीय विधानमंडल में साम्प्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया गया।
- सभी प्रांतों को विभिन्न सम्प्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
- अन्य शेष मतदाता, जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया।
- बम्बई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से सात स्थान मराठों के लिये आरक्षित कर दिये गये।
- विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिये दोहरी व्यवस्था की गयी। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया गया।
- सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों के निर्वाचन का अधिकार बना रहा।
- दलित जातियों के लिये विशेष निर्वाचन की यह व्यवस्था बीस वर्षों के लिये की गयी।
- दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गयी।
कांग्रेस का पक्ष यद्यपि कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी किंतु अल्पसंख्यकों से विचार-विमर्श किये बिना वह इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी। इस प्रकार साम्प्रदायिक निर्णय से गहरी असहमति रखते हुये कांग्रेस ने निर्णय किया कि वह न तो साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगी न ही इसे अस्वीकार करेगी।
साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा, दलितों को सामान्य हिन्दुओं से पृथक कर एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप मे मान्यता देने तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सभी राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया।
गांधीजी की प्रतिक्रिया
गांधीजी ने साम्प्रदायिक निर्णय की राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। उनका मत था कि यह हिन्दुओं एवं दलित वर्ग दोनों के लिये खतरनाक है। उनका कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। एक बार यदि पिछड़े एवं दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अश्पृश्यता को दूर करने का मुद्दा पिछड़ा जायेगा और हिन्दू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचक मंडल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर न ही विधानमंडलों या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है और न ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की। अपितु सबसे मुख्य जरूरत समाज से अश्पृश्यता की कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की है।
गांधीजी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्म-निर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तथापि उन्होंने दलित वर्ग के लिये बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया। अपनी मांगों को स्वीकार किये जाने के लिये 20 सितंबर 1932 से गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गये। कई राजनीतिज्ञों ने गांधीजी के अनशन को राजनीतिक आंदोलन की सही दिशा से भटकना कहा। इस बीच विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेता, जिनमें एम.सी. रजा, मदनमोहन मालवीय तथा बी.आर. अम्बेडकर सम्मिलित थे, सक्रिय हो गये। अंततः एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या पूनापैक्ट के नाम से जाना जाता है।
पूना समझौता
सितंबर 1932 में डा. अम्बेडकर तथा अन्य हिन्दू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिन्दुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार-
- दलित वर्ग के लिये पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिन्दुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गये।
- लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या 47 से बढ़कर 147 कर दी गयी।
- मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18, बम्बई एवं सिंध में 15-15, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिये सुरक्षित किये गये।
- केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिये संयुक्त व्यवस्था को मान्यता दी गयी।
- दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गयी।
सरकार ने पूना समझौते को साम्प्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया।
गांधीजी का हरिजन अभियान
सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पुन पैक्ट के द्वारा हिन्दुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधीजी को बुरी तरह आहत कर दिया था। फिर भी गांधीजी ने पूना समझौते के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किये जाने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधीजी ने अपने अन्य कार्यों को छोड़ दिया तथा पूर्णरूपेण ‘अश्पृश्यता निवारण अभियान’ में जुट गये। उन्होंने अपना अभियान यरवदा जेल से ही प्रारंभ कर दिया था तत्पश्चात अगस्त 1933 में जेल से रिहा होने के उपरांत उनके आदोलन में और तेजी आ गयी।
अपनी कारावास की अवधि में ही उन्होंने सितम्बर 1932 में ‘अखिल भारतीय अश्पृश्यता विरोधी लीग’ का गठन किया तथा जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। जेल से रिहाई के उपरांत वे सत्याग्रह आश्रम वर्धा आ गये। साबरमती आश्रम, गांधीजी ने 1930 में ही छोड़ दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि स्वराज्य मिलने के पश्चात ही वे साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) में वापस लौटेंगे। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधीजी ने अपनी ‘हरिजन यात्रा‘ प्रारंभ की। नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक गांधीजी ने पूरे देश की यात्रा की तथा लगभग 20 हजार किलोमीटर का सफर तय किया। अपनी यात्रा के द्वारा गांधीजी ने स्वयं द्वारा स्थापित संगठन ‘हरिजन सेवक संघ’ जगह-जगह पर कोष एकत्रित करने का कार्य भी किया। गांधीजी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था-हर रूप में अश्पृश्यता को समाप्त करना। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया की गांवों का भ्रमण हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का कार्य करें। दलितों को ‘हरिजन’ नाम सर्वप्रथम गांधीजी ने ही दिया था। हरिजन उत्थान के इस अभियान में गांधीजी 8 मई व 16 अगस्त 1933 को दो बार लंबे अनशन पर बैठे। उनके अनशन का उद्देश्य, अपने प्रयासों की गंभीरता एवं अहमियत से अपने समर्थकों को अवगत कराना था। अनशन की रणनीति ने राष्ट्रवादी खेमे को बहुत प्रभावित किया। बहुत से लोग भावुक हो गये।
अपने हरिजन आंदोलन के दौरान गांधीजी को हर कदम पर सामाजिक प्रतिक्रियावादियों तथा कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ प्रदर्शन किये तथा उन पर हिंदूवाद पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया गया। सविनय अवज्ञा आदोलन तथा कांग्रेस का विरोध करने के निमित्त, सरकार ने इन प्रतिक्रियावादी तत्वों का भरपूर साथ दिया। अगस्त 1934 में लेजिस्लेटिव एसेंबली में ‘मंदिर प्रवेश विधेयक’ को गिराकर, सरकार ने इन्हें अनुग्रहित करने का प्रयत्न किया। बंगाल में कट्टरपंथी हिन्दू विचारकों ने पूना समझौते द्वारा हरिजनों को हिन्दू अल्पसंख्यक का दर्जा दिये जाने की अवधारणा को पूर्णतयाः खारिज कर दिया।
गांधी जी के जाति संबंधी विचार
गांधीजी ने अपने पूरे हरिजन आंदोलन, सामाजिक कार्य एवं अनशनों में कुछ मूलभूत तथ्यों पर सर्वाधिक जोर दिया-
- हिन्दू समाज में हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचार तथा भेदभाव की उन्होंने तीव्र भर्त्सना की।
- दूसरा प्रमुख मुद्दा था- छुआछूत को जड़ से समाप्त करना। उन्होंने अश्पृश्यता की कुरीति को समूल नष्ट करने तथा हरिजनों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिये जाने की मांग की।
- उन्होंने इस बात की मांग उठायी कि हिन्दुओं द्वारा सदियों से हरिजनों पर जो अत्याचार किया जाता रहा है, उसे अतिशीघ्र बंद किया जाना चाहिए तथा इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए। शायद यही वजह थी कि गांधीजी ने अम्बेडकर या अन्य हरिजन नेताओं की आलोचनाओं का कभी बुरा नहीं माना। उन्होंने हिन्दू समाज को चेतावनी दी कि “यदि अश्पृश्यता का रोग समाप्त नहीं हुआ तो हिन्दू समाज समाप्त हो जायेगा। यदि हिंदूवाद को जीवित रखना है तो अश्पृश्यता को समाप्त करना ही होगा”।
- गांधीजी का सम्पूर्ण हरिजन अभियान मानवता एवं तर्क के सिद्धांत पर अवलंबित था। उन्होंने कहा कि शास्त्र छुआछूत की इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन यदि वे ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं तो हमें उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना मानवीय प्रतिष्ठा के विरुद्ध है।
गांधीजी अस्पृश्यता निवारण के मुद्दे को अंतर्जातीय विवाह एवं अंतर्जातीय भोज जैसे मुद्दों के साथ जोड़ने के पक्षधर नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि ये चीजें स्वयं हिन्दू सवर्ण समाज एवं हरिजनों के बीच में भी हैं। उनका कहना था कि उनके हरिजन अभियान का मुख्य उद्देश्य, उन कठिनाइयों एवं कुरीतियों को दूर करना है, जिससे हरिजन समाज शोषित और पिछड़ा है।
इसी तरह उन्होंने जाति निवारण तथा छुआछूत निवारण में भी भेद किया। इस मुद्दे पर वे डा. अम्बेडकर के इन विचारों से असहमत थे कि छुआछूत की बुराई जाति प्रथा की देन है तथा जब तक जाति प्रथा बनी रहेगी यह बुराई भी जीवित रहेगी। अतः जाति प्रथा को समाप्त किये बिना अछूतों का उद्धार संभव नहीं है। गांधीजी का कहना था कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई पाप नहीं है। हां, छुआछूत अवश्य पाप है। उनका तर्क था कि छुआछूत, जाति प्रथा के कारण नहीं अपितु ऊच-नीच के कृत्रिम विभाजन के कारण है। यदि जातियां एक दूसरे की सहयोगी एवं पूरक बन कर रहें तो जाति प्रथा में कोई दोष नहीं है। कोई भी जाति न उच्च है न निम्न। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक एवं विरोधियों दोनों से आह्वान किया कि वे आपस में मिलकर काम करें क्योंकि दोनों ही छुआछूत के विरुद्ध हैं।
गांधीजी का विचार था कि छुआछूत की बुराई का उन्मूलन करने से उसका साम्प्रदायिकता एवं ऐसे ही अन्य मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसकी उपस्थिति का तात्पर्य होगा जाति प्रथा में उच्च एवं निम्न की अवधारणा को स्वीकार करना। गांधीजी ने छुआछूत के समर्थक दकियानूसी प्रतिक्रियावादी हिन्दुओं को ‘सेनापति‘ कहा। किंतु वे इन पर किसी प्रकार का दबाव डाले जाने के विरोधी थे। उनका कहना था कि इन्हें समझा-बुझाकर तथा इनके दिलों को जीतकर इन्हें सही रास्ते पर लाना होगा न कि इन पर दबाव डालकर। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अनशन का उद्देश्य, उनके द्वारा चलाये जा रहे छुआछूत विरोधी आंदोलन के संबंध में उनके मित्रों एवं अनुयायियों के उत्साह को दुगना करना है।
अभियान का प्रभाव
गांधीजी ने बार-बार यह बात दुहराई कि उनके हरिजन अभियान का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है अपितु यह हिन्दू समाज एवं हिन्दुत्व का शुद्धीकरण आंदोलन है। वास्तव में गांधीजी ने अपने हरिजन अभियान के दौरान केवल हरिजनों के लिये ही कार्य नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया कि जनआंदोलन के निष्क्रिय या समाप्त हो जाने पर वे स्वयं को किस प्रकार के रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। उनके आंदोलन ने राष्ट्रवाद के संदेश को हरिजनों तक पहुंचाया। यह वह वर्ग था, जिसके अधिकांश सदस्य खेतिहर मजदूर थे तथा धीरे-धीरे किसान आंदोलन तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे।
रणनीति पर बहस
सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के उपरांत राष्ट्रवादियों के मध्य भविष्य की रणनीति के संबंध में द्वि-स्तरीय बहस प्रारंभ हुई-प्रथम, निकट भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति कैसी हो तथा द्वितीय, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत होने वाले 1937 के आगामी प्रांतीय चुनावों में, सत्ता में भागेदारी के प्रश्न पर किस रणनीति का अनुगमन किया जाये।
प्रथम चरण की व्याख्या
इस चरण में तीन अवधारणायें सामने आयीं। इनमें से प्रथम दो परम्परागत प्रतिक्रियावादी अवधारणायें थीं, जबकि तीसरी, कांग्रेस में सशक्त वामपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये तीनों अवधारणायें निम्नानुसार थीं-
- पहली अवधारणा के अनुसार, गांधीवाद की तर्ज पर रचनात्मक कार्य प्रारंभ किया जाये।
- दूसरी अवधारणा के अनुसार, एक बार पुनः संवैधानिक तौर-तरीकों से संघर्ष प्रारंभ करना चाहिए। इस मत के समर्थक 1934 के भावी केंद्रीय विधान सभा के लिये होने वाले चुनावों में भाग लेने का भी समर्थन कर रहे थे। इस मत के समर्थकों में आसफ अली, सत्यमूर्ति, डा. एम.ए. अंसारी, भूलाभाई देसाई तथा बी.सी. राय प्रमुख थे। इन सभी का मत था कि-
राजनीतिक निराशा के इस दौर में, जबकि कांग्रेस जन-आंदोलन जारी रखने की अवस्था में नहीं हैं, उसे चुनावों में भाग लेकर विधानमंडल में प्रवेश करना चाहिए तथा राजनीतिक संघर्ष जारी रखना चाहिए, जिससे जनता का मनोबल गिरने न पाए।
चुनाव में भाग लेने का तात्पर्य यह नहीं है कि वे केवल संवैधानिक राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब एक अन्य राजनीतिक मोर्चा प्रारंभ करना है।
इस नये राजनीतिक मोर्चे से कांग्रेस मजबूत होगी, जनता में उसका प्रभाव बढ़ेगा तथा जनता अगले दौर के आंदोलन के लिये तैयार हो सकेगी।
विधान मंडल में कांग्रेस की उपस्थिति उसे नये राजनैतिक संघर्ष के लिये उपयुक्त मंच प्रदान करेगी।
- तीसरी अवधारणा का समर्थन कांग्रेस का सशक्त वामपंथी विचारों का समर्थक दल कर रहा था, जिसका नेतृत्व नेहरू के हाथों में था। यह गुट सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेकर उसके स्थान पर रचनात्मक कार्य प्रारंभ करने तथा विधान मंडल में भागेदारी, दोनों मतों का विरोधी था।
इनका मत था कि ये दोनों तरीके जन-आंदोलन को उसके पथ से विमुख कर देंगे तथा उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान दूसरी ओर मोड़ देंगे। ये जन-आंदोलन को जारी रखने के पक्षधर थे। इनका मानना था कि आर्थिक संकट का यह दौर क्रांतिकारी आंदोलन का उचित समय है तथा जनता संघर्ष के लिये पूरी तरह तैयार है।
नेहरू के विचार
नेहरू ने कहा कि “न केवल भारतीय जनता अपितु पूरे विश्व की जनता के सम्मुख इस समय मुख्य लक्ष्य पूंजीवाद का समूल उन्मूलन तथा समाजवाद की स्थापना है”। नेहरू के विचार से सविनय अवज्ञा आदोलन को वापस लेना, रचनात्मक कार्य प्रारंभ करना तथा संसद में भागेदारी करना एक प्रकार की आध्यात्मिक पराजय, आदर्शा का समर्पण तथा क्रातिकारी पथ का परित्याग कर सुधारवादी पथ को अपनाने जैसा था।
उन्होंने सुझाव दिया कि समाज के वर्गीय चरित्र की वास्तविकता और वर्ग संघर्ष की महत्ता को स्वीकार करते हुये समाज के स्वार्थपरक तत्वों को जनसाधारण के हितों की ओर मोड़ा जाना चाहिए। जमीदारों तथा पूंजीपतियों के विरुद्ध मजदूरों तथा किसानों के संघर्ष तथा उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि मजदूरों और किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित किया जाए जिससे कांग्रेस इन संगठनों की गतिविधियों एवं नीतियों को निर्देशित कर सके। नेहरू का मानना था कि वर्ग संघर्ष के अभाव में वास्तविक साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता।
नेहरू द्वारा संघर्ष-समझौता-संघर्ष की रणनीति का विरोध
गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक बड़े तबके का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध पहले संवैधानिक तरीके से जबरदस्त संघर्ष प्रारंभ करके आदोलन अचानक वापस ले लिया जाये, फिर सरकार के सुधारवादी कदमों से समझौता कर पुनः समय आने पर संघर्ष प्रारंभ कर दिया जाए। क्योंकि तीव्र संघर्ष के पश्चात् संघर्ष के सुप्तावस्था में आने पर जनसामान्य को अपनी सार्मथ्य बढ़ाने का मौका मिलेगा तथा सरकार को राष्ट्रवादी मांगों का प्रत्युत्तर देने का अवसर दिया जा सकेगा। जनसामान्य को अनिश्चितकालीन बलिदान की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन यदि सरकार ने राष्ट्रवादी मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो जनसाधारण को पूरे सामर्थ्य से पुनः संघर्ष प्रारंभ कर देना चाहिए। इसे ही ‘संघर्ष-समझौता-संघर्ष की रणनीति’ कहते हैं।
नेहरू, संघर्ष-समझौता-संघर्ष की इस रणनीति से असहमत थे। उन्होंने तर्क दिया कि लाहौर अधिवेशन में पूर्णस्वराज्य के कार्यक्रम को तय किये जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया है, जहां हमें उपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष करते रहना होगा, जब तक कि हम उसे पूर्णरूपेण उखाड़ फेंकने में सफल न हो जायें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस को ‘निरंतर संघर्ष की नीति’ का पालन करना चाहिए तथा उसे साम्राज्यवादी ढांचे से सहयोग एवं समझौते के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की चेताया कि अत्यंत शक्तिशाली औपनिवेशिक सत्ता को आने-चार आने की ताकत द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। अपितु इसके लिये सतत संघर्ष अपरिहार्य है। उन्होंने संघर्ष-समझौता-संघर्ष की रणनीति का विरोध करते हुये उसके स्थान पर संघर्ष-विजय की रणनीति का प्रतिपादन किया।
अंततः सत्ता में भागेदारी पर सहमति
इस समय भारतीय राष्ट्रवादी जहां एक ओर असमंजस की स्थिति में थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत यह मानकर चल रही थी कि कांग्रेस में सूरत विभाजन की तरह शीघ्र ही एक और विभाजन होना लगभग तय है। किंतु इस अवसर पर गांधीजी ने दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाकर कांग्रेस को विभाजित होने से बचा लिया। यह जानते हुए भी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रमुख और एकमात्र तरीका सत्याग्रह ही है, उन्होंने कॉसिलों में भागेदारी के समर्थकों की मांगे स्वीकार कर लीं। उन्होंने कहा कि “संसदीय राजनीति से स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती किंतु वे सभी कांग्रेस जन जो न तो स्वयं को रचनात्मक कार्यों में लगा सकते और न ही सत्याग्रह में भाग ले सकते, वे सभी संसदीय राजनीति के माध्यम से स्वयं को सक्रिय बनाये रख सकते हैं बशर्ते कि वे संविधानवादी या सुविधावादी न बन जायें”। साथ ही गांधीजी ने वामपंथियों को आश्वस्त करते हुये भी कहा कि “सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना आवश्यक एवं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में उचित कदम था, लेकिन इसका तात्पर्य राजनीतिक अवसरवादिता के सम्मुख समर्पण या साम्राज्यवाद से समझौता नहीं है”।
मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन पटना में हुआ, जहां चुनाव में भाग लेने के लिये एक संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। गांधीजी ने महसूस किया कि कांग्रेस में उभर रही सबसे सशक्त धारा से वह कट से गये हैं। वे जानते थे कि बुद्धजीवी वर्ग का एक बड़ा तबका संसदीय राजनीति के पक्ष में है, जबकि वे मौलिक तौर पर संसदीय राजनीति के विरोधी थे। बुद्धिजीवी वर्ग का दूसरा खेमा गांधी जी के रचनात्मक कार्यो यथा-चरखा कातने इत्यादि से असहमत था, जिसे गांधीजी ‘राष्ट्र का दूसरा हृदय’ कहते थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समाजवादी गुट भी गांधीजी की नीतियों से असहमत था। इसी कारण 1934 में गांधीजी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वे “कांग्रेस एवं उसमें उभरती नयी विचारधारा पर नैतिक दबाव डालकर उसे रोकना नहीं चाहता क्योंकि यह मेरे अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है”।
नेहरू और समाजवादियों ने भी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। कांग्रेस के विरोधियों का मत था कि नेहरू एवं समाजवादियों के द्वारा कांग्रेस में किये जा रहे मौलिक परिवर्तनों से कांग्रेस विभाजित हो जायेगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नेहरू एवं समाजवादियों ने इस खतरे को भांपकर अपनी प्राथमिकतायें तय कर लीं। उनका मत था कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उपनिवेशी शासन को समाप्त करना आवश्यक है तथा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में कांग्रेस का सहयोग करना जरुरी है। क्योंकि कांग्रेस ही भारतीयों का एकमात्र प्रमुख संगठन है।
नेहरू एवं समाजवादियों का तर्क था कि वैचारिक या राजनीतिक शुद्धीकरण के नाम पर कांग्रेस से त्यागपत्र देने या उससे नाता तोड़ने की बजाय कांग्रेस में रहकर उसे जुझारू चरित्र प्रदान करना कहीं ज्यादा आवश्यक है। दक्षिणपंथियों ने भी इस मसले पर सही रणनीति अपनायी। नवंबर 1934 में केंद्रीय विधान सभा के लिये हुये चुनाव में कांग्रेस ने प्रशंसनीय प्रदर्शन करते हुये भारतियों के लिये आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें जीत लीं।